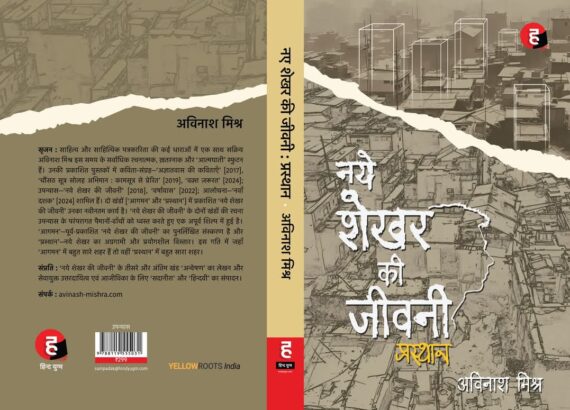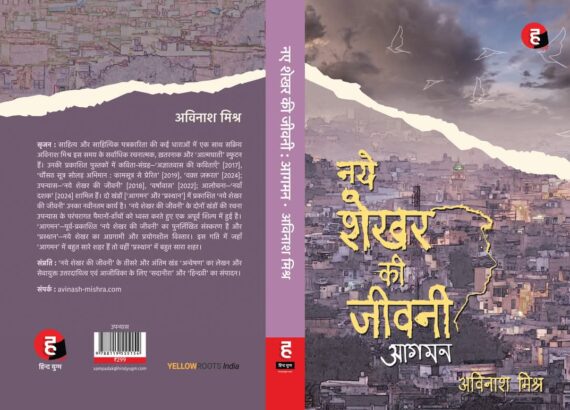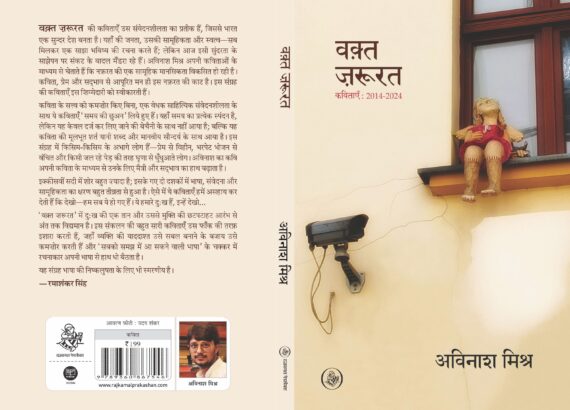औरत के अपमान की कहानियाँ जलाने को

मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास ‘फ़रिश्ते निकले’ की संरचना एक लाक्षागृह सरीखी है। औरत के अपमान की कई कहानियाँ इसमें स्वरूप लेती हैं। लेकिन इन कहानियों की शक्ति यह है कि ये कोई साहसवंचित सहानुभूति नहीं उपजातीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने निष्कर्षों और बनत में बग़ावती हैं। यातनाएँ इस उपन्यास में मौजूद नायिकाओं की अदम्य जिजीविषा, संकल्पों, संघर्षों, स्वप्नों और लड़ाइयों को कमज़ोर नहीं कर पातीं। वे एक रोज़ इस लाक्षागृह से बाहर निकलती हैं और इसमें आग लगा देती हैं। ‘दि फ़ीमेल यूनॅक’ से जर्मेन ग्रीयर के शब्द यहाँ मौक़े का उद्धरण होंगे कि ये नायिकाएँ ‘पुराने प्रक्रम का नवीनीकरण नहीं करना है, उसे तोड़ना होगा’ इस लक्ष्य के क्रियान्वयन का प्रतीक हैं।
उपरोक्त अनुच्छेद के बाद प्रस्तुत उपन्यास की समीक्षा कुछ तात्कालिक हुआ चाहती है। बिल्कुल नज़दीक से गुज़रे वक़्त में इस समाज में मर्दानगी के कुछ ऐसे विकृत और नए नमूने सार्वजानिक हुए हैं, जिन्होंने मनुष्यता को शर्मसार किया है। एक ऐसे दौर में जब आरोपियों और दोषियों से ज़्यादा प्राचीन हो गया है यह कहना कि बख़्शा नहीं जाएगा, संवेदनशीलता सिर्फ़ शर्म से सिर झुकाकर रह जाती है। इन वहशी घटनाओंकी—जिन्हें बार-बार बलात्कार कहकर संबोधित किया जाता है—जड़ें कहाँ हैं? इस पर विमर्श के लिए एक पूरा तंत्र विकसित हो चुका है जो प्रत्येक बलात्कार के बाद उपचारिक नहीं औपचारिक रूप से प्रस्तुत होता है। यह कहना कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन बलात्कार की बेशुमार घटनाएँ और उनसे संबंधित ख़बरें स्त्री-अस्मिता के मूल संघर्ष और स्वर को कमज़ोर कर रही हैं। समानता के शोर के बीच स्त्रियों को शत्रुओं की तरह रौंदते-कुचलते हुए पुरुषों की सोच बदल नहीं रही है; वे अपनी हैवानियत में अब भी निर्भय, असभ्य और बर्बर हैं :
‘‘मगर बात यह भी भूलने की नहीं है कि लड़कियाँ और औरतें इनसे शरीर में नुकीले सरिया फँसे होने के बावजूद लड़ती हैं। जब तक जान रहती है, वे सुस्त नहीं होतीं; मात नहीं खातीं। तभी तो हारकर इन दरिंदों को उन जाँबाज़ लड़कियों की हत्या करनी पड़ती है।’’ [ पृष्ठ : 100 ]
मैत्रेयी पुष्पा की कथा-सृष्टि की नायिकाएँ जाँबाज़ रही आई हैं। ‘दि सब्जेक्शन ऑफ़ विमेन’ में आए जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि इन नायिकाओं के लिए ‘नैतिकता की असली कसौटी है, बुराई को निरुत्साहित करने की क्षमता।’ उन्हें घेरकर उनका बार-बार बलात्कार किया जा सकता है, उन्हें लहूलुहान किया जा सकता है, इसके बाद भी अगर वे बच गईं तब उन्हें ज़लील किया जा सकता है… बावजूद इसके ये नायिकाएँ सतही और भावुकतापूर्ण ढंग से पेश नहीं आतीं—ये लड़ने, लड़ते रहने और जीतने की मिसाल क़ायम करने में यकीन रखती हैं।
‘साइकोलॉजी ऑफ़ सेक्स’ के लेखक हैवलाक एलिस ने विवाह के कारण होने वाले बलात्कारों की संख्या को संख्या में दूसरे बलात्कारों से ज़्यादा बताया था। लेकिन बेला बहू विवाह-संस्था के भीतर भी उत्पीड़ित हैं और बाहर भी। बेला बहू ‘फ़रिश्ते निकले’ की मुख्य किरदार हैं, लेकिन यह उपन्यास कुछ इस बनत का है कि इसमें किरदार में से किरदार में से किरदार… निकलते चले जाते हैं। इसके ही एक किरदार जुझार सिंह के शब्दों में कहें तो समझिए कि ‘अत्याचार, अन्याय और बलात्कार के सारे मॉडल यहाँ इकट्ठे हैं।’ बेला की कथा के विस्तार में जाने से बचने के लिए यहाँ केवल यह कहा जा सकता है कि बेला के जीवन और फूलन देवी के जीवन में कई समानताएँ हैं। लेकिन अपने मूल उद्देश्य में बेला का जीवन—ऐसी स्थितियों से ग्रस्त स्त्रियों के लिए—फूलन के जीवन से ज़्यादा अनुकरणीय है :
‘‘बेला, फूलन देवी का क़िस्सा सुने या आपबीती दोहराए या कि आँखों से भस्म कर देने वाली, कई-कई हाथों से दुष्ट-दलन करने वाली दुर्गा का मनन करे?उसे पक्का विश्वास हो गया है कि देवी किसी मंदिर या मढ़िया में नहीं होतीं, वे बीहड़ घाटियों में रहती हैं फूलन बनकर। वे समाज में रहती हैं डायन बनकर, वे घरों में रहती हैं चुड़ैल बनकर और वे रसूख़वालों के बीच रहती हैं बेला बनकर।’’ [ पृष्ठ : 86 ]
बेला अपने अपमान की कहानियों को जलाने के बाद क़ानून के आगे आत्म-समर्पण कर देती है। जेल में उसकी मुलाक़ात फूलन देवी से होती है और उनसे उसे कुछ अचूक मंत्र मिलते हैं, जैसे :
‘‘समाज को बाग़ी औरतें ही बदल सकती हैं, ‘भली’ औरतों को मर्द गन्ने की तरह पेरते रहते हैं।’’
‘‘मर्दों के पीछे दौड़ना छोड़ो औरतो, उनको अपने स्वाभिमान और सम्मान के पीछे दौड़ाओ। तुम मर्दों से ज्यादा योग्य हो क्योंकि जद्दोजहद के साथ हमदर्दी की मालकिन हो। मगर अपना ग़ुस्सा पीने के लिए नहीं उगलने के लिए बचाकर रखो। औरत के ग़ुस्से की आग में मर्दों के ग़ुरूर और मालिकाना संस्कार भस्म हो जाएँगे।’’ [ पृष्ठ : 87 ]
जेल से रिहाई के बाद ‘मैं कहां जाऊँगी अब?’ यह सवाल बेला बहू के सामने साँप के फन-सा खड़ा हो जाता है। यहाँ आकर मशहूर ईरानी फ़िल्मकार ज़फ़र पनाही की ईरान में प्रतिबंधित रही आई फ़िल्म ‘दि सर्कल’ स्मृत हो उठती है। इस फ़िल्म की नायिकाओं का जीवन इतना नारकीय हो चुका है कि जेल की दुनिया उन्हें बाहर की दुनिया से बेहतर लगती है। यह फ़िल्म इस पड़ाव पर आकर ख़त्म होती है कि स्त्रियों के लिए असली जेल तो मर्दों की बनाई वह दुनिया है जिससे बग़ावत करने के जुर्म में उन्हें ये जेल नसीब हुई है। इससे मुक्त होने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक मर्दों की बनाई दुनिया से रिहाई नहीं मिलती, क्योंकि इस रिहाई के लिए फिर बग़ावत होगी और लौटकर फिर यहीं आना होगा। इस तरह ग़ुलामी और क़ैद का एक वर्तुल पूरा होता है।
लेकिन मैत्रेयी पुष्पा के माध्यम से अभिव्यक्त बेला की रिहाई उसे मर्दों की बनाई इस दुनिया में—वापस जेल की ओर नहीं—अपने ही जैसे सताए गए लोगों के बीच ले जाती है। इन लोगों का रिकार्ड शराफ़त से दूर रहने का रहा है। अजय सिंह ने सज़ा काटी है तो जुझार सिंह भी डकैती की ट्रेनिंग पाया हुआ छोटा डाकू है। बसंती घर से भागी हुई लड़की है, उसे डकैतों को खाना पहुँचाने का बहुमूल्य अनुभव है। गुलाब सरकारी कारतूसों का कुशल दलाल रहा है। उजाला, जिसके साथ बलात्कार हुआ, लोहापीटाओं की छोकरी है जो दो बलात्कारियों की मर्दानगी की चटनी बना आई है। इन सब किरदारों और इनसे भी जुड़े किरदारों का जीवट भरा जीवन इस उपन्यास को प्रेरणादायक और सकारात्मक प्रभाव में विन्यस्त करता है। बदलाव की उम्मीद के प्रति समर्पण के साथ शुरू हुआ यह उपन्यास धीरे-धीरे बदलाव और उम्मीद की ओर बढ़ता है और अंत तक आते-आते अपने पढ़ने वाले को बदलाव और उम्मीद से भर देता है।
‘उपन्यास-लेखन पर उपन्यासकार के लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है?’ इस प्रश्न पर थोड़ा गहराई से सोचते हुए ‘ए रूम ऑफ़ वंस ओन’ में वर्जीनिया वुल्फ़ कहती हैं, ‘केवल उपन्यास के विषय में सोचें तो यह ऐसी रचना दिखाई पड़ेगा जिसमें जीवन दर्पण की तरह दिखाई पड़ता है, हालाँकि इसमें असंख्य सामान्यताएँ और विकृतियाँ भी होती हैं। …इसके मूल्य वास्तविक जीवन के मूल्य होते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के मूल्य पुरुषों द्वारा निर्मित मूल्यों से प्राय: भिन्न होते हैं।’ इस उद्धरण के आलोक में कहें तो कह सकते हैं कि मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासकार की रसाई स्त्री-अस्मिता के महत्त्वपूर्ण इलाक़ों तक है। वह इस दृष्टि को मूल्यनिष्ठ होकर कथा में कुछ इस क़दर बसाने का हुनर जानती हैं कि वह वास्तविक यथार्थ से क़तई विच्छिन्न नहीं होती। स्त्री को अपनी मिल्कियत समझने वाली पुरुष-मानसिकता के मूल्यों से मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासकार के मूल्य कैसे भिन्न हैं, इसकी नज़ीर के लिए प्रस्तुत उपन्यास के एक पुरुष किरदार अजय सिंह के हिस्से आए संवाद को उद्धृत करना पर्याप्त होगा :
‘‘अपने समाज में यह बात बड़े प्रामाणिक तरीके से सिद्ध की जाती है कि औरत अक्सर ही बड़ी हैसियत वालों, दौलतमंदों और बड़ी जाति वालों को अपनी जवानी का लालच दिखाकर फाँस लेती है, जिसे वे नादान मोहब्बत समझ लेते हैं। मोहब्बत की बेड़ियाँ बड़ी कसावट वाली होती हैं। आदमी दिखाता है कि पुरानी आशनाई ख़त्म हो गई मगर भीतर ही भीतर उस पर कुढ़ता रहता है। यही कारण है कि इस इश्क़ के ज़ोर का हथियार खानदान तक को नहीं छोड़ता। ज़ाती दुश्मन हो जाते हैं मर्द नाम के इंसान। और तब ये औरतें अपनी जीत का आनंद लेती हैं। डंकिनी-शंखिनी, दूती, कुटनी औरतों की कहानियाँ ऐसी ही हैं।’’ [ पृष्ठ : 215 ]
सती, देवी, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी, अर्द्धांगिनी, अनुगामिनी… इन ‘अच्छे-अच्छे’ नामों का फ़रेब मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में बार-बार खुलता आया है। ‘दि सेकेंड सेक्स’ में सीमोन द बोउवार ने सेक्सुअलिटी को केवल अस्तित्व का एक पहलू भर बताया है। लेकिन मैत्रेयी पुष्पा की नायिकाएँ सेक्सुअलिटी को अपनी मुक्ति का मार्ग मानती आई हैं। इस मार्ग में यह उपन्यास लेखिका की तरफ़ से इस नज़रिए से भी नया है, क्योंकि इसमें न केवल ‘अच्छे-अच्छे’ नामों का फ़रेब खुलता है; बल्कि सेक्सुअलिटी का फ़रेब भी खुलता है। इस तरह के खुलासों में लेखिका का यक़ीन इस वजह भी उल्लेखनीय है, क्योंकि सारे युक्ति-तर्क इसका समर्थन करते हैं।
सीमोन ने ही ‘दि सेकेंड सेक्स’ में ‘स्त्रियों के बीच सामूहिकता की भावना का अभाव है’ इस तथ्य को रेखांकित किया था। ‘फ़रिश्ते निकले’ इस तथ्य को धुंधला करता है। यह घृणित राजनीति और बुरे अर्थ में बदलते मूल्यों वाले एक पतित परिदृश्य में पारस्परिकता और स्त्रियों के बीच सामूहिकता की भावना को ऊँचाई देता है। मेहनत की तौहीन और हुनर की बेक़दरी को इसमें पढ़ना और सहना आसान नहीं है, अपने असर में यह पाठ बेचैन कर देने वाला है। लेकिन इसके बीच ही यह एकजुटता और परोपकार की ज़रूरत भी समझता है। यह अब्राहम लिंकन की इस बात को उद्धृत करता है कि ‘ग़ुंडों से डर मत जाना क्योंकि उनको झुकाना सबसे आसान होता है’ और अंत में उनके मशहूर ‘प्रधानाध्यापक के नाम पत्र’ से समाप्त होता है, यह कहना ग़लत होगा क्योंकि महत्त्वपूर्ण कृतियाँ जहाँ ख़त्म होती जान पड़ती हैं; दरअस्ल, वहीं वह आधारभूत शुरुआत होती है जो पाठकों का हृदय छू लेती है।
‘पाखी’ (जुलाई-2014) में पूर्व-प्रकाशित।